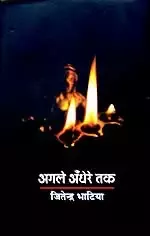|
कहानी संग्रह >> अगले अँधेरे तक अगले अँधेरे तकजितेन्द्र भाटिया
|
453 पाठक हैं |
||||||
कहानी संग्रह
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी कहानी में विज्ञान के अनुशासनों से
आने वाले लेखकों में जितेन्द्र
भाटिया सबसे महत्त्वपूर्ण कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ अपनी संरचना में
‘फार्म इन पोर्स’ की सार्थक अन्विति लगती हैं। इनमें
भाषा के भीतर की कोई अनियन्त्रित आकुलता नजर आती है, जिसे सुविचारित ढंग
से वे आकार देते रहते हैं।
प्रस्तुत संकलन के लिए चुनी गई जितेन्द्र भाटिया की इधर की कहानियों में उनका एक दूसरा, अलबत्ता कहना चाहिए, अधिक गंभीर और विवेकशील रूप दिखाई देता है। इनमें उनकी पिछली कहानियों की तरह महानगर और उसका संश्लिट यथार्थ तो उसी तरह बरकरार है, लेकिन एक दृष्टि में इनमें कहीं ज्यादा सार्थकता और विविधता है।
जितेन्द्र के भीतर एक बेचैन कथाकार की आत्मा मौजूद है जो दुनिया को एक ध्रुवीय बनाने तथा उसके जाल को बिछाने वाली ताकतों को बहुत करीब से देखता है और समझता है। ये कहानियाँ अपने ढंग की ऐसी अलग कहानियाँ हैं, जो कथा-प्रयोगों की मारामारी के बीच भी अपनी पाठनीयता से पाठक का ध्यान आकर्षित करती हैं।
जितेन्द्र भाटिया की ये कहानियाँ अपने वक्त से संवाद करने के साथ ही उन नुक्तों का भी विश्लेष्ण करती हैं जिनसे जीवन का कार्य-व्यवहार संचालित होता है। उनमें चेतना-विहीन समय में चेतना जगाने के साथ ही, लेखक के शब्दों में, ‘आदमी को जमीन के आखिरी बेशकीमती टुकड़े’ को बचाने की ईमानदार कोशिश भी नजर आती है।
प्रस्तुत संकलन के लिए चुनी गई जितेन्द्र भाटिया की इधर की कहानियों में उनका एक दूसरा, अलबत्ता कहना चाहिए, अधिक गंभीर और विवेकशील रूप दिखाई देता है। इनमें उनकी पिछली कहानियों की तरह महानगर और उसका संश्लिट यथार्थ तो उसी तरह बरकरार है, लेकिन एक दृष्टि में इनमें कहीं ज्यादा सार्थकता और विविधता है।
जितेन्द्र के भीतर एक बेचैन कथाकार की आत्मा मौजूद है जो दुनिया को एक ध्रुवीय बनाने तथा उसके जाल को बिछाने वाली ताकतों को बहुत करीब से देखता है और समझता है। ये कहानियाँ अपने ढंग की ऐसी अलग कहानियाँ हैं, जो कथा-प्रयोगों की मारामारी के बीच भी अपनी पाठनीयता से पाठक का ध्यान आकर्षित करती हैं।
जितेन्द्र भाटिया की ये कहानियाँ अपने वक्त से संवाद करने के साथ ही उन नुक्तों का भी विश्लेष्ण करती हैं जिनसे जीवन का कार्य-व्यवहार संचालित होता है। उनमें चेतना-विहीन समय में चेतना जगाने के साथ ही, लेखक के शब्दों में, ‘आदमी को जमीन के आखिरी बेशकीमती टुकड़े’ को बचाने की ईमानदार कोशिश भी नजर आती है।
मैं और मेरा समय
ज़मीन के आखिरी टुकड़े तक
(लेखकीय)
मुझसे मिलकर अक्सर लोगों का भ्रम टूटता है। साहित्यकारों को मैं काफी
अविशिष्ट, खामोश या (नकारात्मक अर्थों में) बहुत
‘सम्भ्रान्त’ नजर आता हूँ और पैसे वाले
‘सम्भ्रान्तों’ को बेहद फक्कड़ अथवा फटीचर। पाठकों को
मुझमें लेखकीय गुणों का अभाव दिखाई देता है, और जिनका साहित्य से कहीं दूर
का भी रिश्ता नहीं है, वे सब समझते हैं कि मैं जरूरत से ज्यादा
गैर-दुनियादार और अव्यावहारिक व्यक्ति हूँ। इन सारी धारणाओं के बीच सचमुच
मेरा अपना क्या है, यह सोचने बैठूँ, तो भी एक बहुत चलताऊ, मीडियॉकर किस्म
की तस्वीर के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। यानी तमाम दूसरे लोगों की तरह मेरे
भीतर भी अपनी ही तरह के विरोधाभास हैं। इर्दगिर्द की दुनिया के प्रति बेहद
सेंसिटिव होते हुए भी मैं हद दर्जे का आत्मकेन्द्रित व्यक्ति हूँ। काम को
लेकर बेहद मेहनती और अनुशासित होने के बावजूद मुझे लीक से हटना अच्छा लगता
है। और जिन दूसरों से मैं सीखता हूँ, ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, उन्हीं के लिए
अक्सर मेरे पास बहुत कम वक्त होता है। इन्हें आप मेरी स्वार्थपरकता की
सीमारेखाएँ या मेरे दोगलेपन के ‘कोऑर्डिनेट्स’; कुछ
भी कह सकते हैं। बाहर परिवेश से अलग आपकी अन्दरूनी दुनिया में भी
अनुभूतियों का एक बहुरंगी मोजेक होता है। जमाने के दुःख-दर्द अपनी जगह
हैं, परन्तु इनके समानान्तर खाने, उठने, बैठने सोने या काम करने की स्तव्य
और नामालूम दिनचर्या के बीच भीतर का यह मोजेक न जाने कितने सन्दर्भहीन
अक्स बनाता-उभारता रहता है। बड़ी और अनिवार्य चिन्ताओं से अलग अनुभव और
व्यक्तित्व के इस ‘रैडम’ अन्दरूनी हिस्से का अवचेतन
मन की किसी मनोवैज्ञानिक ग्रन्थि से भी जोड़ना मुश्किल होगा। मसलन चलती
गाड़ी के सींखचों पर कसी नन्ही-नन्ही उँगलियाँ। बर्फ से ढँके टीलों पर
धँस-धँसकर उभरते भारी, वजनदार कदम। बर्फ, जो मैंने कभी नहीं देखी। पुरानी
दिल्ली के प्लेटफार्म पर भूसे में लिपटी आमों की पेटियों की पुरअसरार
खुशबू। क्रिकेट के आफ स्पिन में घूमता हाथ। बड़ी ऊँगली से बार-बार हवा में
बनती तीन की आकृति, जिसे बस, में सामने की सीट पर कण्डक्टर से झगड़ता
बूढ़ा एक झटके के साथ तोड़ देता है। ‘लाइफ’ मैगजीन
में बरसों पहले देखा एक खूबसूरत जादूगरनी का चेहरा। मेरे जन्म से कोई तीन
दशक पहले मर चुके पगड़ीधारी दादा की डीएवी कॉलेज लाहौर की लाइब्रेरी के
बाहर खिंचवाई गई आखिरी तस्वीर यह सब भी मेरे अनुभव संसार का एक जरूरी
हिस्सा है। इसे आप क्या कहेंगे ?
किसी एक शब्द का नाम लो, अगर कहा जाए तो यात्रा और संक्रमण, जो मेरे रचना संसार का एक जरूरी हिस्सा है, मेरे लिए इसी बेचैनी के पर्याय हैं और इस बेचैनी के बगैर दुनिया की किसी भी चीज का रचा जाना शायद असंभव है। जरा देर के लिए अगर लेखक, समाज, पाठक, दायित्व, प्रतिबद्धता, पक्षधरता आदि जुमलों से अलग हटकर आदमी के अन्दरूनी अकेलेपन की बात की जाए तो चीजें एकाएक खामोशी में तब्दील होने लगेंगी। इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं अपने आपको एक बेहद कमजर्फ, असहिष्णु और नाखुश व्यक्ति पाता हूँ। कदम-कदम पर अपने परिवेश से ‘कम्यूनिकेट’ करने की कोशिश में छटपटाता, बार-बार शंकित नजरों से इर्दगिर्द देखकर अपने चारों तरफ मोटे खोल गिराता और रह-रह कर इन खोलों की दीवारों को तोड़कर दुबारा बाहर धूप में उतरता और पसीने में चिपचिपाता। इस अंदरूनी व्यक्ति के लिए ‘आत्म’ या अहम् के तहत कोई अतिरिक्त सम्मान का भाव मेरे मन में नहीं है, पर इसका रोजमर्रापन और शिनाख्त के लिए शिद्दत से छटपटाना मुझे सहज ही एक आत्मीयता से भर देता है। इस आदमी को मैं जानता हूँ। इसकी कमजोरियाँ, कामयाबियाँ, नाकामयाबियाँ मेरी पहचानी हुई हैं। इसके साथ मैंने अपनी संवादहीनता को झेला है। यह मैं हूँ।
फिल्मकार गुरदत्त अपने जमाने के युवा वर्ग के लिए एक अच्छा-खासा हीरो बनकर मरा था। खिंची हुई त्योरियों के नीचे उसकी स्वयं के ही भीतर झाँकती अनुभवसम्पन्न आँखें परिवेश द्वारा सताये हुए संवेदनशील आदमी की जीती-जागती मिसाल बन गयी थीं। यही आदमी सड़कों पर आवारा घूमता था, चकलों और कोठों की खस्ता हालत पर फिकरे कसता था, व्यक्तिपूजक समाज का मजाक उड़ाता था अन्ततः ‘ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है’ और ‘बिछुड़े सभी बारी-बारी’ के साथ डायरेक्टर की कुर्सी पर मरा हुआ पाया जाता था। यही आत्मोन्मुख पात्र जब आगे चल कर स्वयं पर जरूरत से ज्यादा तरस खाने लगा तो धीरे-धीरे उसका पतन भी शुरू हुआ। लेकिन महत्त्वपूर्ण यह है कि जिस पात्र का मूल संघर्ष था अपने परिवेश के साथ ही सामंजस्य स्थापित कर पाना। और यहीं से यह पात्र बेहतर सामाजिक और संगत होने लगता था। अपने भीतर झाँकते-झाँकते वह वैसी ही जिन्दगी जी रहे लाखों युवकों की बेचैनी के सक्षम स्वर देता महसूस होता था...
मिसाल सन्दर्भहीन लग सकती है, लेकिन कैशोर्य के भावुक क्षणों में गुरुदत्त का यही पात्र मेरी भीतरी दुनिया के चोर दरवाजे तक भी आया है। परन्तु एक ओर जहाँ मैं गुरुदत्त की मूल व्यथा से अपने आपको जोड़ सका हूँ, वहीं दूसरी ओर इस पात्र के आत्म करुण लहजे और जमाने द्वारा समझे न जाने के गुरूर ने मुझे मोहभंग की स्थिति में भी डाला है। आदमी यह अपेक्षा क्यों रखता है कि उसके संपर्क में आने वाले लोग हमेशा उसे ही समझेंगे ? अकेला छूट गया आदमी अपने-आपको विशिष्ट क्यों मानने लगता है ?....
बेचैनी एक आदर्श रचना-स्थिति है, मैं कह रहा था। दरअसल रचना को जन्म देने वाले इस व्यक्तिगत अकेलेपन की शिनाख्त करते हुए मैं स्वयं अपने में भी बहुत साफ नहीं हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे अनुभव के झोले में एहतियात से सँभाले गये वे व्यक्तिगत दस्तावेज हरगिज नहीं है, जिनके आधार पर लोग अक्सर अपने लिखे हुए के लिए सबूत या ‘जस्टिफिकेशन’ पेश करते हैं। दिग्गज लिक्खाड़ों या जुमलों का व्यापार करने वाले लफ्फाजों की तरह मजमा जुटाने के लिए मेरे पास भूतपूर्व प्रेमिकाओं या दिलफेंक प्रशंसिकाओं की कोई वर्णक्रमानुसार सूची भी नहीं है। अपनी पैरवी के लिए तकलीफ अथवा संघर्ष के किसी भव्य, अचम्भे में डाल देने वाले अनुभव-संसार को जुटा पाने में भी मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। बल्कि दुःख भरे दिनों की यादों के बीच से भी मैंने कोई छोटा या बड़ा स्मृतिशेष पाया है, जिसके समाप्त हो जाने का अहसास मन को एक अजीब से खालीपन से भर गया है। मेरी गुजरी हुई जिन्दगी की धूल भरी तहों में कहानीकार के ‘जीन्स’ शायद कहीं नहीं मिलेंगे। वक्त की मार ने मुझे अपने-आपको अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर किया है, ऐसा कोई सोचा हुआ सुविधाजनक झूठ भी मेरे पास नहीं है।
तो फिर ?...किसी स्पष्ट या समझ में आने वाले सीधे उत्तर के नाम पर मेरे पास यही परिचित-सी बेचैनी और खलिश है, जिसे तोड़ने का एकमात्र रास्ता मेरे लिए अनिवार्यतः ‘लिखे हुए शब्द’ से होकर गुजरता है....
आदमी आखिर अपनी जिन्दगी से क्या चाहता है, या कि यह जिन्दगी आदमी से कौन-कौन-सी अपेक्षाएँ रखती है ? अपनी कहानी ‘सिद्धार्थ का लौटना’ के नायक की तरह यह सवाल मैंने कई बार अपने-आपसे पूछा है। लेकिन हर बार एक नामालूम से अपराध-बोध के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है और मैं अक्सर अपनी लिखी हुई फिजूल-सी पंक्तियाँ काटकर खामोश हो गया हूँ।
दुःख और संघर्ष का जिक्र एक ‘क्लिशे’ है क्योंकि तकलीफ हर आदमी झेलता है। दुःख को गुरुदत्त की तरह गौरवान्वित करना कहीं उसकी आन्तरिक गरिमा और ऊर्जा को नष्ट कर डालना भी है, क्योंकि दुःख छोटा या बड़ा नहीं, सिर्फ दुःख होता है। दुःख आपको जो कुछ देता है, उसे बगैर बेईमानी किये शब्दों में ढालकर दूसरों के साथ बाँटना बड़े जोखिम का काम है। इसमें दूसरे बहुत दूर छूट जाते हैं और खुद अपनी ही नजरों में गिर जाने का तात्कालिक मगर गम्भीर खतरा लगातार सामने बना रहता है...।
चेतना की शुरुआत राजस्थान के उस छोटे से कस्बे से मानी जा सकती है। रेत के टीले। भुतहा नीम का पेड़। कीकर की झाड़ियाँ। बीमारी। माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त...वही सब। जिन्दगी की तमाम अच्छी चीजों का शौकीन यह फलता-फूलता पंजाबी परिवार उस रेत और अन्धड़ भरे इलाके में क्या कर रहा था जहाँ दिन में बीस घण्टे धूल भरी लू कहर बरसाती थी ?...शायद इस परिवार को खुद भी नहीं मालूम, पर जिन्दगी की तमाम गर्दिश रोजी-रोटी की तलाश का पर्याय बन गयी थी और एक बहुत बड़ा हादसा किसी डरावनी छाया की तरह हाल में ही पीछे छूटा था।
मैंने अपनी आँखों से बटवारे को नहीं देखा, लेकिन मैंने भाभीजी (दादी) की आँखें देखी हैं। उनका सब-कुछ लाहौर की गलियों में पीछे छूट गया था...सूत्तर मण्डी का बड़ा-सा पुश्तैनी घर, पड़ोस, बाजार, पति की यादें...सभी कुछ। माँ ने अपनी एक बहन को खोया था। इसके अलावा छोटे-बड़े व्यक्तिगत हादसे थे, जिनका जिक्र हम बच्चों के सामने कम ही होता था। लेकिन भाभीजी की तकलीफ इन हादसों से कहीं बड़ी थी जहाँ एक ओर उम्र के आखिरी पड़ाव पर बँटवारे ने उन्हें अपने परिचित संस्कृति और सामाजिक माहौल से –जबर्दस्ती, बेरहमी के साथ बेदखल कर दिया था, वहीं दूसरी ओर उनका अपना परिवार (जिसमें बुआएँ चाचा और उनके बच्चे शामिल थे) इस जलजले के फौरन बाद लावारिसों की तरह देश के छोटे-बड़े कस्बों में बिखर गया था। बेशक पिता ने कम उम्र में दादा की मृत्यु के बाद से ही इस पूरे परिवार को बच्चों की तरह पाला था, लेकिन उनकी और भाभीजी की व्यथा में काफी फर्क था। पिता के सामने जहाँ अब एक लम्बी उतार-चढ़ावों से भरपूर जिन्दगी बाकी थी, वहीं दादा के दामन में खूबसूरत अतीत की तकलीफदेह यादों के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था...
सांस्कृतिक संकट क्या होता है ? क्या यह कि लाहौर से कुछ शरणार्थी भागे थे और भारत आकर अलग-अलग शहरों कस्बों की गलियों में एक नये सिरे से जिन्दगी से जूझने लगे थे ? या यह कि चार-पाँच साल का एक बच्चा दादी की गोद में बैठा बबूल के काँटों पर मुँह मारते ऊँटों का सीधा अनुभव अपनी आँखों में सँजोए लाहौर की सूत्तर मण्डी की शान-शौकत, वहाँ के दोमंजिला मकान, वहाँ के अतुलनीय कुल्फी वालों की जादुई कहानियाँ सुनता था और तय नहीं कर पाता था कि इनमें से कौन-सी दुनिया उसकी अपनी है ?....
बचपन के उन प्रारम्भिक दिनों में ही मैंने जाना था कि भाभी जी की सीमित शब्दावली में ‘पाकिस्तान’ से बदसूरत कोई शब्द नहीं है। व्यक्तिगत हादसों से गुजरी आर्यसमाजी माँ कभी-कभी भावातिरेक में ‘रुड़ जाने मूसले’ और इसी तरह की दूसरी कड़वी शब्दावली में बँटवारे के लिए जिम्मेदार लोगों का जिक्र करती थीं, पर भाभीजी की स्मृतियों में वे क्षण रह-रहकर ताजा हो उठते थे जब उनके गाँव के मुसलमान उनके घरों में शादी-ब्याह में रिश्तेदारों की तरह शरीक होते थे। और विदाई के वक्त हिन्दू बेटियों के लिए फूट-फूटकर रोते थे...संकट शायद यह भी था कि ‘पाकिस्तान’ नामक अकेले शब्द ने एक झटके के साथ इस सारी गुँथी हुई संस्कृति को हमेशा के लिए अविश्वास और नफरत की भट्टी में झोंक दिया था और दादी इस परिवर्तन को आत्मसात कर पाने में असमर्थ, भीतर-ही-भीतर घुटती चली गयी थीं। आज अगर मेरी दादी जिन्दा होतीं और ऐटमी धमाकों में गुत्थमगुत्था और लहूलुहान दोनों मुल्कों की जद्दोजहद को देखतीं तो पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजरती....
बँटवारे की विभीषिका के बाद से जहाँ एक ओर पंजाबी कौम का उद्यमी मिजाज और प्रतिकूल जीवन स्थितियों में लड़ते चले जाने का जुझारूपन उभरकर सामने आया है, वहीं दूसरी ओर अभावों का स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी जिन्दगी खालिस भौतिक जरूरतों के इर्दगिर्द चक्कर लगाते दिखाई देने लगी है। सीमित साधनों के एक उखड़े हुए परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने आर्थिक विपन्नता को बहुत नजदीक से देखा है। घर का अंकगणित रुपयों, आनों और पैसों के इर्दगिर्द घूमता था और हमारी बालसुलभ सीमित दुनिया में तब ‘पीला टका’ (दो पैसे) दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद समझा जाता था। हमारी इस तंग जिन्दगी के समानान्तर दूसरे शहरों और कस्बों में दादी के अन्य रिश्तेदार और बिरादरीवाले भी इसी तरह की सख्त लड़ाई से गुजरते हुए किसी अजनबी मिट्टी में अपने पाँव जमाने के लिए संघर्षरत थे। ‘हान्जी’, ‘आहोजी’, ‘भ्राजी’, ‘बाश्शाओ’, और ‘भाप्पाजी’ की उस खलिस पंजाबी-सुलभ चाटुकारिता और व्यापारकुशलता की सीढ़ियाँ लगाकर हर कोई जल्दी-से-जल्दी उस पुरानी खुशहाली को दुबारा मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता था...
‘चार पैसे की लड़ाई’ के इस मुश्किल दौर में जब पिता ने अपने आत्मसम्मान के तहत बरसों की बँधी-बँधाई नौकरी बिना किसी विकल्प के इन्तजार किये एकाएक छोड़ दी थी तो दिल्ली के सदर बाजार से आगरे की ‘राजे दी मण्डी’ तक फैली तमाम बिरादरी की आँखें-फटी-की-फटी रह जाना स्वाभाविक था। आश्चर्यजनक यह भी था कि कई वर्षों तक पनाह देने वाले उस कस्बे की ओर पिता ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था और न ही अपने निर्णय को लेकर किसी तरह का कोई अफसोस मन में आने दिया था। इस असाधारण फैसले के बाद घरेलू झगड़ों की आड़ में रिश्तेदारों और सगे-संबंधियों के तमाम चेहरे अजनबियों में तब्दील हो गये थे और बनजारों की सी सहजता से सारा माल-असबाब ट्रक पर लादकर हम सब जयपुर चले आये थे...
जयपुर का वह छोटा-सा किराये का मकान, मिट्टी की मेड़ से घिरा दिगम्बर जैन विद्यालय, मान प्रकाश सिनेमा के सामने गैस के हण्डों तले बिकती गँडेरियों के मोहक ढेर, स्टैच्यू सर्कल की लम्बी, वीरान शामें और झुटपुटे में घर की सीढ़ियों पर हथेलियों के बीच चेहरा टिकाकर बैठे पिता की आकृति...ये सब जयपुर के उस साल भर के प्रवास की पुरअसरार तस्वीरें हैं, जिन्हें भुला सकना मुश्किल हैं। सी स्कीम का वह इलाका, जहाँ हमने अभावों की उस सख्त धूप को झेला था, अब पर्यटकों की गुलाबी नगरी का एक भव्य हिस्सा बन चुका है, जिसमें से उस पुरानी, जर्जर तस्वीर को ढूँढ़ निकालना शायद असम्भव होगा....
दस भूखे आश्रितों का घर चलाने वाले एक अकेले मध्यमवर्गीय पंजाबी के लिए सालभर तक बेकार रहने का मतलब क्या होता है ? शायद बहुत कुछ, परन्तु दुःख और अभाव ने हमें एक अदृश्य सूत्र में बाँध दिया था। पिता के सामने एक वर्ष के दौरान समझौतों के कई अवसर आये, पर वे ‘पंजाबी दी नाक्क’ को पूरी तरह चरितार्थ करते अपनी शर्तों पर जहाँ-के-तहाँ बने रहे और अर्थकेन्द्रित माहौल के आदी बने मेरे अपरिपक्व मन को पहली बार पता चलना शुरू हुआ कि आदमी के माथे पर खिंची आत्मसम्मान की त्यौरियों की कीमत कभी-कभी तमाम भौतिक सुविधाओं से कहीं ज्यादा बैठती है....
और उसके बाद दिल्ली। बेगैरत नकली व्यवहार और हरामजदगियों के बीच बसा एक संस्कृतिविहीन शहर, जैसा कि मुझे हमेशा लगता है। खालीपन के लम्बे अन्तराल के बाद पिता को शिक्षामन्त्रालय में एक सम्मानजनक नौकरी मिल गयी थी और बड़े भाई को यहीं के एक कॉलेज में लेक्चररशिप। दिल्ली में मेरा पहला परिचय सर्दियों की दोपहर में कमलानगर के मेले ग्राउण्ड में फैली ‘चारपाई सभ्यता’ से हुआ था, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति हर दूसरे आदमी की जिन्दगी में खामख्वाह दखल रखता था। तीस हजारी स्थित स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी कैम्पस तक फैली ‘पुराणी दिल्ली’ की वह जिन्दगी कदम-कदम पर बदकारियों से घिरी थी, जिनसे मेरी पुरातनपन्थी माँ मुझे भरकस बचा लेना चाहती थी। एक बार स्कूल के बंगाली दोस्त संदीप सरकार (यह नाम पता नहीं अब तक कैसे याद है) के घर से जब मैं ‘लूचि’ और ‘मांस’ (से मेरी दादी ‘तरकारी’ कहती थीं) खाकर लौटा था तो उन्होंने तीन दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। परन्तु अपनी समूची वैदिक सदाशयता के बावजूद वे मुझे बर्बाद होने से बचा नहीं सकीं। दिल्ली में कुछ ही महीने गुजारने के बाद मैं अपनी गली में ‘बण्टों’ और ‘ठिक्कर’ (सोडावाटर बोतलों के ढक्कनों से खेला जानेवाला खेल। का बेताज बादशाह बन गया था। मुहल्ले का शहरी गाली-गलौज धीरे-धीरे मेरी जबान पर भी चढ़ने लगा सन बावन के आम चुनावों में मैंने भी बच्चों की टोली के साथ ‘चिह्न हमारे डिब्बे का, दीपक दीपक दीपक है’ चिल्ला-चिल्लाकर खासा यश और लाभ अर्जित किया था।
मेरे अपने सांस्कृतिक ‘विकेन्द्रीकरण’ के साथ-साथ घर के दूसरे सदस्यों पर भी महानगर के सुपरिचित दबाव अपना असर दिखाने लगे थे। दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में धक्के खाने के बाद जब पिता सेक्रेटेरियट से घर लौटते थे तो उन्हें हम बच्चों के साथ अपने अनुभव बाँटने का वक्त ही नहीं मिलता था। यूँ भी बड़े भाई-बहनों की अपनी एक ताजातरीन वयस्क दुनिया थी जिसमें डूब चुकने के बाद उनमें हमारे प्रति एक अनकही हिकारत का सा भाव जागने लगता था। कुल जमा स्थिति यह थी कि सालभर के उस छोटे से अर्से में ही दिल्ली की जहरीली हवा ने हमारे पूरे परिवार के सांस्कृतिक ढाँचे को बेतरह तहस-नहस कर दिया था...माँ इस बीच चोरी-छिपे उस कस्बे की शान्त जिन्दगी को याद कर लेती थीं, जिसे पिता ने एक झटके के साथ तोड़ दिया था और दादी दिल्ली तथा लाहौर के सारे साम्य और ‘जात-बिरादरी’ के पड़ोस के बावजूद ‘सत्तूर मण्डी’ के उस फिक्सेशन से मुक्त नहीं हो पाती थीं जिसके अन्तर्गत लाहौर में हमारी ‘ऐड्डी वड्डी कोठी’ हुआ करती थी। पिता ने अपनी जिन्दगी में हार मानना नहीं सीखा था लेकिन दिल्ली की धक्का-मुक्की और दौड़-भाग उन्हें भी कहीं गहरे में तोड़ने लगी थी।
बचपन के उन दो वर्षों के अनुभव के कारण ही मैं आज तक दिल्ली के नाम से घबराता हूँ क्योंकि कमलानगर की वे घुटनभरी दीवारें ही मेरे लिए इस शहर का पर्याय बन चुकी हैं। दिल्ली का औसत आदमी आज भी मेरे मन में मक्कारी और पंजाबी ‘रिफ्यूजी-सुलभ’ आत्मपरकता की एक पेटेण्ट तश्वीर पेश करता है। रेस्त्राओं और सार्वजनिक स्थलों पर यहाँ लोग तफरीह के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर अपने कपड़ों, अपने पैसों और अपने अक्खड़पन का रौब गालिब करने जाते हैं। चापलूसी और झूठी तारीफ की सतह को नाखून से जरा-सा खुरचते ही यहाँ इन्सान का खुदगर्ज और ‘डॉग ईट डॉग’ वाला बेमुरव्वत चेहरा दिखाई देने लगता है। शायद बँटवारे के बाद के वर्षों में इन लोगों ने यह सारा खुदरापन विकसित किया है, लेकिन स्कूटरों पर ऑफिस बैग लटकाए भीड़ में से गुजरते कुकरेजा, मखीजा, ‘सैक्ट्री साब’, ‘शाहजी‘, ‘होरजी’ और ‘टीटू दी गड्डी’ का यह चलतापुर्जा शहर मुझे कभी रास नहीं आया और न ही शायद कभी भविष्य में आएगा। पुराने दिल्लीवासी माफ करेंगे, लेकिन यदाकदा इस शहर में पहुँचकर जब मुझे नयी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी जाने के लिए ऑटो लेना होता है तो रास्ते भर यह डर बना रहता है कि अभी इसका बददिमाग ड्राइवर किसी अन्धी गली में रिक्शा मोड़कर मुझे मुहल्लेवालों से पिटवा देगा या फिर ‘वन-वे’ का बहाना कर मुझे कनॉट प्लेस से कनॉट प्लेस के सर्कुलर रूट पर चक्कर कटवाता रहेगा।
मेरे बचपन की अधिकांश याद रहने वाली घटनाएँ किसी-न-किसी रूप में यात्रा से जुड़ी है। सम्भवतः यही कारण है कि यात्रा और ‘ट्रांजिशन’ मेरी कहानियों में लगभग एक किरदार की हैसियत से आते हैं। इधर पिछले चार-पाँच वर्षों में काम के सिलसिलें में मैंने इतनी अधिक यात्राएँ की हैं कि नजदीक के लोगों को आश्चर्य होता है। लेकिन इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी सबसे साफ तौर पर याद है कि ट्रेन का वह खूबसूरत सफर, जो हमने दिल्ली से कलकत्ता जाते हुए तय किया था। अलीगढ़ से कुछ आगे रेलवे लाइन के बराबर पक्की दीवार के पीछे फैले अमरूदों के बाग, कानपुर के प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले छोटे-छोटे तिकोने समोसों का स्वाद झाझा स्टेनशन पर आधी रात के वक्त बदले जाते इंजन से आसमान में चाँद पर उठता काला धुआँ और गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर बदहवाश दौड़ते पैरों की आहट....ये सारे बिम्ब मेरे जेहन की तख्ती पर अपनी स्थायी जगह बना चुके हैं...
पिता के तबादले के साथ दिल्ली छोड़कर कलकत्ता आना हम सबके लिए एक विराट अनुभव था क्योंकि सारी गरीबी, खस्ताहाली और गन्दगी के बावजूद कलकत्ता में जिन्दगी की एक उनमुक्त, ताजगीभरी धड़कन थी, जिसे दिल्ली की गला काटने वाली संस्कृति से अलग पहचाना जा सकता था।
आज भी अगर मुझे अपनी गुजरी हुई पूरी जिन्दगी में से कोई छोटा-सा कालखण्ड चुनने के लिए कहा जाए तो मैं बेहिचक हिन्दुस्तान पार्क और बालीगंज में गुजरे उन पाँच वर्षों की खातिर अपनी सारी उम्र को दाँव पर लगाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। कलकत्ता छोड़ने के सोलह लंबे वर्षों के बाद मैं किसी गवेषक की तरह सुधा को साथ लिए उन्हीं परिचित गलियों और सड़कों पर खोये स्मृति चिह्नों की तलाश में बेमतलब यहाँ से वहाँ तक भटका, लेकिन उस गुजरे हुए कालखण्ड को दुबारा जी पाना सम्भव नहीं हुआ। शायद सोलह वर्षों के इस भयावह अन्तराल में वह मासूम दृष्टि, जो जिन्दगी की मामूली खूबसूरतियों को पकड़ पाने के लिए जरूरी होती है, हमसे हमेशा के लिए छीन ली गयी थी...
हिन्दुस्तान पार्क के हमारे दोमंजिला मकान की बगल में खानदानी बंगाली रईसों की एक आलीशान कोठी थी, जिसके लम्बे-चौड़े बगीचे में खूबसूरत गार्डन-चेयर्स पर बैठे मर्द-औरतों के प्रति हम बच्चों के मन में एक अजीब से कौतूहल का भाव जागता था। कौन हैं ये लोग जो सुबह-शाम चाँदी के चमचमाते टी-सेट्स पर चाय पीते हैं और कुर्सी के नीचे हरी घास पर लोट लगाते रोयेंदार कुत्तों का माथा सहलाते हैं। क्या करता है बरामदे की झूलेदार कुर्सी पर बैठकर सिगार पीता वह बूढ़ा, जिसकी बेटी हर रोज रंगीन पाड़ वाली झक्क सफेद कलफ लगी सूती साड़ी पहनकर बेथुन कॉलेज की बस में पढ़ने जाती है। कहाँ गुम हो जाते हैं वे ढेर-ढेर ‘डाब’ जिन्हें छुट्टी वाले दिन माली उस बगीचे के अनगिनत नारियल के पेड़ों से उतारकर घास पर एक कोने में इकट्ठा करता है ? बंगाली आभिजात्य का वह संयत, मगर रौबीला प्रदर्शन हर रोज हमारी आँखों के सामने होता था। और हम हर बार सोचते कि इन खुशकिस्मत लोगों की तरह हमारे घरों में भी क्यों सुबह-शाम बाघबाजार के राजभोगों की हाँडियाँ नहीं आती और क्यों हम भी उन लोगों की तरह दिल बहलाने के लिए घर में तीन-तीन ‘कॉकर स्पेनियल’ कुत्ते नहीं पाल सकते ?
वैसे जिन्दगी हमारी भी ‘दारुण’ मजे की थी, इसमें कोई शक नहीं। घर के बरामदे में एक बड़ा-सा जंगला था जिसके ठीक सामने से एक सड़क आकर हमारी सड़क से मिलती थी। अँग्रेजी के ‘टी’ के केन्द्रबिन्दु पर स्थित घर का बरामदा हमारे लिए घण्टों के लम्बे बालसुलभ मनोरंजन का जरिया बन जाता था। शाम ढलने के बाद जब अँधेरा सिमटता था तो बहन के साथ एक विचित्र होड़ में मैं उस जंगले की सलाखों पर अपना सिर गड़ा लेता था। सामने की एक सड़क से आती कार की हर हेडलाइट के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। कार अगर दायें मुड़ती थी तो ‘प्वाइण्ट’ बहन को मिलता था। और बायें मुड़नेवाली कार मेरे हिस्से में आती थी...
हम बच्चों के लिए बालीगंज लोकल स्टेशन के ओवरब्रिज पर खड़े होकर नीचे से गुजरती ट्रेनों को देखना एक और जरूरी शगल था। हड़ताल वाले दिन रासबिहारी ऐवेन्यू की खुली सड़क के बीचोंबीच ट्रामलाइन की घास पर क्रिकेट जमती थी...इसके अलावा रोइंग क्लब के पीछे झील में बने टापू तक जाते ‘हिलनेवाले पुल’ के नीचे पानी में चने फेंकते ही उन्हें निगलने के लिए छटपटाती सैकड़ों बड़ी-बड़ी मछलियाँ...और गरियाहट चौराहे से देशप्रिय पार्क तक कि वह आये दिन की बिना टिकट ट्राम यात्रा, साउथ एण्ड स्टोर्स के भीतर ताजा घुटी कॉफी की पुरअसरार महक या उससे और आगे गरियाहट के बाजार में बिकते दरियाई कछुओं के रस्सी से बँधे छोटे-छोटे पैर...उस दुनिया ने न जाने कितने सारे अविस्मरणीय अक्स हमारी चमकती आँखों में हमेशा के लिए कैद कर दिये थे...
घोष ब्रदर्स और साउथएण्ड स्टोर्स से कुछ आगे निकलने पर मिलने वाला वह तिकोना पार्क अब भी वहीं है, लेकिन उसके अंदर फैले कूड़े के अस्तव्यस्त ढेर में से कागज तलाशते भिखारियों को देखते हुए अब कहीं भीतर, बहुत गहरे में कुछ टूटता-सा महसूस होता है...
हमारे मकान मालिक एक बुजुर्ग थे, जिनकी पोती एक फालिज के मारे बेटे से हमारी खासी दोस्ती हो गई थी। काली पूजा के दिन उनके घर में बाहर के दरवाजे से लेकर सीढ़ियोंसे होते हुए भी भीतर तक सफेद ‘अल्पना’ से लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाये जाते थे, ताकि दिवाली की रात अगर लक्ष्मी भीतर आने का इरादा रखें तो उन्हें रास्ता ढूढ़ने में कठिनायी न हो। बहुत-सी रातें हमने उस चमत्कारिक देवी की आहटों के इन्तजार में बितायी थीं, लेकिन वे कभी नहीं आयीं और हमारे मकान मालिक ‘दादू’ के मकान की दूसरी मंजिल यूँ ही बरसों तक अधूरी, अधबनी हालत में मरम्मत और पलस्तर का इन्तजार करती रही...
कालीघाट के मोड़ पर जब ट्राम ‘बाटा’ की दुकान के सामने से होती हुई ‘रस्सा रोड’ के स्टॉप पर रुकती थी तो एक बूढ़ा भिखारी अनिवार्यतः ट्राम के जंगले से सट जाया करता था। ‘‘अन्धा के दया करुन, भोगोबान मंगल कोरबे...’’ उसकी परिचित आवाज ट्राम के भीतर गूँजती थी और काली मंदिर की दिशा में संस्कारगत हाथ जोड़ने वाले बंगाली अकसर कुछ-न-कुछ दे देते थे...इस धर्मपरायणता से काफी दूर आठवीं कक्षा के झोपड़ीनुमा क्लासरूम में हमारे सबसे प्रिय अध्यापक उत्पल दत्त (बाद में विख्यात अभिनेता और नाटककार) मुँह में मोटा सिगार दबाये हमें रोनाल्ड रिडआउट की ‘इंग्लिश टुडे’ से अँग्रेजी का पाठ पढ़ाते थे और गाहे-ब-गाहे किसी एक विद्यार्थी को खड़ा कर यह भी पूछ लेते थे कि उसने लाइट हाउस, सिनेमा में लगी ‘यूलिसेस’ फिल्म अब तक क्यों नहीं देखी !..,.यह उत्पल दत्त के ओजस्वी स्वर में सिखाये गये अँग्रेजी साहित्य की विलक्षणताओं के उस पहले सबक का ही चमत्कार था कि मैं रातोंरात बच्चों की परी कथाओं से आगे निकलकर केनेथ ग्रैहम की ‘विण्ड इन दि विलोज’ और विलियम गोल्डिंग की ‘लॉर्ड ऑफ़ दि फ्लाइज’ पर उतर आया था और आगे चलकर हिन्दी माध्यम से हायर सैकेण्ड्री करने के बावजूद मुझे अपनी अँग्रेजी को लेकर कभी हीनता का अहसास नहीं हुआ...
कोई पच्चीस वर्ष गुजर जाने के बाद एक बार जब मैंने प्लेन में अपनी बगल में बैठे शख्स को उत्पल दत्त के रूप में पहचाना था तो मेरे मुँह से अनायास ही ‘गुडआफ्टरनून सर !’ निकल गया था। वे कुढ़कर मेरी ओर पलटे थे और गुस्से से अँग्रेजी में बोले ते कि मैं क्या आपको ‘सर’ दिखाई देता हूँ ? लेकिन जब मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि ‘सर’ सम्बोधन का इस्तेमाल मैंने अपने उस गुरू के लिए किया था जिसने मुझे आठवीं कक्षा में अँग्रेजी सिखाई थी तो वह अनायास ही पिघल गये थे। बम्बई से कलकत्ता की सारी यात्रा के दौरान वे मेरे साथ साउथप्वाइंट स्कूल की उन यादों को ताजा करते थे और फिर आखिरकार दमदम हवाई अड्डे पर जब हम उतरे थे तो चलते-चलते उन्होंने इतने पुरातन ढंग से मेरे सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया था कि मेरे पास उनके पैर छूने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था। उस वक्त लगा था कि चुरुट मुँह में दबाकर अँग्रेजी पढ़ाने वाले उस रौबीले सूटधारी अध्यापक के भीतर कहीं एक अत्यन्त संवेदनशील, दकियानूसी बंगाली का हृदय भी था और बाहर से भीतर तक की यह दुरंगी विविधता ही कमोबेश मेरे बचपन के उस कलकत्ता की वास्तविक पहचान थी...
किसी एक शब्द का नाम लो, अगर कहा जाए तो यात्रा और संक्रमण, जो मेरे रचना संसार का एक जरूरी हिस्सा है, मेरे लिए इसी बेचैनी के पर्याय हैं और इस बेचैनी के बगैर दुनिया की किसी भी चीज का रचा जाना शायद असंभव है। जरा देर के लिए अगर लेखक, समाज, पाठक, दायित्व, प्रतिबद्धता, पक्षधरता आदि जुमलों से अलग हटकर आदमी के अन्दरूनी अकेलेपन की बात की जाए तो चीजें एकाएक खामोशी में तब्दील होने लगेंगी। इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं अपने आपको एक बेहद कमजर्फ, असहिष्णु और नाखुश व्यक्ति पाता हूँ। कदम-कदम पर अपने परिवेश से ‘कम्यूनिकेट’ करने की कोशिश में छटपटाता, बार-बार शंकित नजरों से इर्दगिर्द देखकर अपने चारों तरफ मोटे खोल गिराता और रह-रह कर इन खोलों की दीवारों को तोड़कर दुबारा बाहर धूप में उतरता और पसीने में चिपचिपाता। इस अंदरूनी व्यक्ति के लिए ‘आत्म’ या अहम् के तहत कोई अतिरिक्त सम्मान का भाव मेरे मन में नहीं है, पर इसका रोजमर्रापन और शिनाख्त के लिए शिद्दत से छटपटाना मुझे सहज ही एक आत्मीयता से भर देता है। इस आदमी को मैं जानता हूँ। इसकी कमजोरियाँ, कामयाबियाँ, नाकामयाबियाँ मेरी पहचानी हुई हैं। इसके साथ मैंने अपनी संवादहीनता को झेला है। यह मैं हूँ।
फिल्मकार गुरदत्त अपने जमाने के युवा वर्ग के लिए एक अच्छा-खासा हीरो बनकर मरा था। खिंची हुई त्योरियों के नीचे उसकी स्वयं के ही भीतर झाँकती अनुभवसम्पन्न आँखें परिवेश द्वारा सताये हुए संवेदनशील आदमी की जीती-जागती मिसाल बन गयी थीं। यही आदमी सड़कों पर आवारा घूमता था, चकलों और कोठों की खस्ता हालत पर फिकरे कसता था, व्यक्तिपूजक समाज का मजाक उड़ाता था अन्ततः ‘ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है’ और ‘बिछुड़े सभी बारी-बारी’ के साथ डायरेक्टर की कुर्सी पर मरा हुआ पाया जाता था। यही आत्मोन्मुख पात्र जब आगे चल कर स्वयं पर जरूरत से ज्यादा तरस खाने लगा तो धीरे-धीरे उसका पतन भी शुरू हुआ। लेकिन महत्त्वपूर्ण यह है कि जिस पात्र का मूल संघर्ष था अपने परिवेश के साथ ही सामंजस्य स्थापित कर पाना। और यहीं से यह पात्र बेहतर सामाजिक और संगत होने लगता था। अपने भीतर झाँकते-झाँकते वह वैसी ही जिन्दगी जी रहे लाखों युवकों की बेचैनी के सक्षम स्वर देता महसूस होता था...
मिसाल सन्दर्भहीन लग सकती है, लेकिन कैशोर्य के भावुक क्षणों में गुरुदत्त का यही पात्र मेरी भीतरी दुनिया के चोर दरवाजे तक भी आया है। परन्तु एक ओर जहाँ मैं गुरुदत्त की मूल व्यथा से अपने आपको जोड़ सका हूँ, वहीं दूसरी ओर इस पात्र के आत्म करुण लहजे और जमाने द्वारा समझे न जाने के गुरूर ने मुझे मोहभंग की स्थिति में भी डाला है। आदमी यह अपेक्षा क्यों रखता है कि उसके संपर्क में आने वाले लोग हमेशा उसे ही समझेंगे ? अकेला छूट गया आदमी अपने-आपको विशिष्ट क्यों मानने लगता है ?....
बेचैनी एक आदर्श रचना-स्थिति है, मैं कह रहा था। दरअसल रचना को जन्म देने वाले इस व्यक्तिगत अकेलेपन की शिनाख्त करते हुए मैं स्वयं अपने में भी बहुत साफ नहीं हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे अनुभव के झोले में एहतियात से सँभाले गये वे व्यक्तिगत दस्तावेज हरगिज नहीं है, जिनके आधार पर लोग अक्सर अपने लिखे हुए के लिए सबूत या ‘जस्टिफिकेशन’ पेश करते हैं। दिग्गज लिक्खाड़ों या जुमलों का व्यापार करने वाले लफ्फाजों की तरह मजमा जुटाने के लिए मेरे पास भूतपूर्व प्रेमिकाओं या दिलफेंक प्रशंसिकाओं की कोई वर्णक्रमानुसार सूची भी नहीं है। अपनी पैरवी के लिए तकलीफ अथवा संघर्ष के किसी भव्य, अचम्भे में डाल देने वाले अनुभव-संसार को जुटा पाने में भी मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। बल्कि दुःख भरे दिनों की यादों के बीच से भी मैंने कोई छोटा या बड़ा स्मृतिशेष पाया है, जिसके समाप्त हो जाने का अहसास मन को एक अजीब से खालीपन से भर गया है। मेरी गुजरी हुई जिन्दगी की धूल भरी तहों में कहानीकार के ‘जीन्स’ शायद कहीं नहीं मिलेंगे। वक्त की मार ने मुझे अपने-आपको अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर किया है, ऐसा कोई सोचा हुआ सुविधाजनक झूठ भी मेरे पास नहीं है।
तो फिर ?...किसी स्पष्ट या समझ में आने वाले सीधे उत्तर के नाम पर मेरे पास यही परिचित-सी बेचैनी और खलिश है, जिसे तोड़ने का एकमात्र रास्ता मेरे लिए अनिवार्यतः ‘लिखे हुए शब्द’ से होकर गुजरता है....
आदमी आखिर अपनी जिन्दगी से क्या चाहता है, या कि यह जिन्दगी आदमी से कौन-कौन-सी अपेक्षाएँ रखती है ? अपनी कहानी ‘सिद्धार्थ का लौटना’ के नायक की तरह यह सवाल मैंने कई बार अपने-आपसे पूछा है। लेकिन हर बार एक नामालूम से अपराध-बोध के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है और मैं अक्सर अपनी लिखी हुई फिजूल-सी पंक्तियाँ काटकर खामोश हो गया हूँ।
दुःख और संघर्ष का जिक्र एक ‘क्लिशे’ है क्योंकि तकलीफ हर आदमी झेलता है। दुःख को गुरुदत्त की तरह गौरवान्वित करना कहीं उसकी आन्तरिक गरिमा और ऊर्जा को नष्ट कर डालना भी है, क्योंकि दुःख छोटा या बड़ा नहीं, सिर्फ दुःख होता है। दुःख आपको जो कुछ देता है, उसे बगैर बेईमानी किये शब्दों में ढालकर दूसरों के साथ बाँटना बड़े जोखिम का काम है। इसमें दूसरे बहुत दूर छूट जाते हैं और खुद अपनी ही नजरों में गिर जाने का तात्कालिक मगर गम्भीर खतरा लगातार सामने बना रहता है...।
चेतना की शुरुआत राजस्थान के उस छोटे से कस्बे से मानी जा सकती है। रेत के टीले। भुतहा नीम का पेड़। कीकर की झाड़ियाँ। बीमारी। माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त...वही सब। जिन्दगी की तमाम अच्छी चीजों का शौकीन यह फलता-फूलता पंजाबी परिवार उस रेत और अन्धड़ भरे इलाके में क्या कर रहा था जहाँ दिन में बीस घण्टे धूल भरी लू कहर बरसाती थी ?...शायद इस परिवार को खुद भी नहीं मालूम, पर जिन्दगी की तमाम गर्दिश रोजी-रोटी की तलाश का पर्याय बन गयी थी और एक बहुत बड़ा हादसा किसी डरावनी छाया की तरह हाल में ही पीछे छूटा था।
मैंने अपनी आँखों से बटवारे को नहीं देखा, लेकिन मैंने भाभीजी (दादी) की आँखें देखी हैं। उनका सब-कुछ लाहौर की गलियों में पीछे छूट गया था...सूत्तर मण्डी का बड़ा-सा पुश्तैनी घर, पड़ोस, बाजार, पति की यादें...सभी कुछ। माँ ने अपनी एक बहन को खोया था। इसके अलावा छोटे-बड़े व्यक्तिगत हादसे थे, जिनका जिक्र हम बच्चों के सामने कम ही होता था। लेकिन भाभीजी की तकलीफ इन हादसों से कहीं बड़ी थी जहाँ एक ओर उम्र के आखिरी पड़ाव पर बँटवारे ने उन्हें अपने परिचित संस्कृति और सामाजिक माहौल से –जबर्दस्ती, बेरहमी के साथ बेदखल कर दिया था, वहीं दूसरी ओर उनका अपना परिवार (जिसमें बुआएँ चाचा और उनके बच्चे शामिल थे) इस जलजले के फौरन बाद लावारिसों की तरह देश के छोटे-बड़े कस्बों में बिखर गया था। बेशक पिता ने कम उम्र में दादा की मृत्यु के बाद से ही इस पूरे परिवार को बच्चों की तरह पाला था, लेकिन उनकी और भाभीजी की व्यथा में काफी फर्क था। पिता के सामने जहाँ अब एक लम्बी उतार-चढ़ावों से भरपूर जिन्दगी बाकी थी, वहीं दादा के दामन में खूबसूरत अतीत की तकलीफदेह यादों के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था...
सांस्कृतिक संकट क्या होता है ? क्या यह कि लाहौर से कुछ शरणार्थी भागे थे और भारत आकर अलग-अलग शहरों कस्बों की गलियों में एक नये सिरे से जिन्दगी से जूझने लगे थे ? या यह कि चार-पाँच साल का एक बच्चा दादी की गोद में बैठा बबूल के काँटों पर मुँह मारते ऊँटों का सीधा अनुभव अपनी आँखों में सँजोए लाहौर की सूत्तर मण्डी की शान-शौकत, वहाँ के दोमंजिला मकान, वहाँ के अतुलनीय कुल्फी वालों की जादुई कहानियाँ सुनता था और तय नहीं कर पाता था कि इनमें से कौन-सी दुनिया उसकी अपनी है ?....
बचपन के उन प्रारम्भिक दिनों में ही मैंने जाना था कि भाभी जी की सीमित शब्दावली में ‘पाकिस्तान’ से बदसूरत कोई शब्द नहीं है। व्यक्तिगत हादसों से गुजरी आर्यसमाजी माँ कभी-कभी भावातिरेक में ‘रुड़ जाने मूसले’ और इसी तरह की दूसरी कड़वी शब्दावली में बँटवारे के लिए जिम्मेदार लोगों का जिक्र करती थीं, पर भाभीजी की स्मृतियों में वे क्षण रह-रहकर ताजा हो उठते थे जब उनके गाँव के मुसलमान उनके घरों में शादी-ब्याह में रिश्तेदारों की तरह शरीक होते थे। और विदाई के वक्त हिन्दू बेटियों के लिए फूट-फूटकर रोते थे...संकट शायद यह भी था कि ‘पाकिस्तान’ नामक अकेले शब्द ने एक झटके के साथ इस सारी गुँथी हुई संस्कृति को हमेशा के लिए अविश्वास और नफरत की भट्टी में झोंक दिया था और दादी इस परिवर्तन को आत्मसात कर पाने में असमर्थ, भीतर-ही-भीतर घुटती चली गयी थीं। आज अगर मेरी दादी जिन्दा होतीं और ऐटमी धमाकों में गुत्थमगुत्था और लहूलुहान दोनों मुल्कों की जद्दोजहद को देखतीं तो पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजरती....
बँटवारे की विभीषिका के बाद से जहाँ एक ओर पंजाबी कौम का उद्यमी मिजाज और प्रतिकूल जीवन स्थितियों में लड़ते चले जाने का जुझारूपन उभरकर सामने आया है, वहीं दूसरी ओर अभावों का स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी जिन्दगी खालिस भौतिक जरूरतों के इर्दगिर्द चक्कर लगाते दिखाई देने लगी है। सीमित साधनों के एक उखड़े हुए परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने आर्थिक विपन्नता को बहुत नजदीक से देखा है। घर का अंकगणित रुपयों, आनों और पैसों के इर्दगिर्द घूमता था और हमारी बालसुलभ सीमित दुनिया में तब ‘पीला टका’ (दो पैसे) दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद समझा जाता था। हमारी इस तंग जिन्दगी के समानान्तर दूसरे शहरों और कस्बों में दादी के अन्य रिश्तेदार और बिरादरीवाले भी इसी तरह की सख्त लड़ाई से गुजरते हुए किसी अजनबी मिट्टी में अपने पाँव जमाने के लिए संघर्षरत थे। ‘हान्जी’, ‘आहोजी’, ‘भ्राजी’, ‘बाश्शाओ’, और ‘भाप्पाजी’ की उस खलिस पंजाबी-सुलभ चाटुकारिता और व्यापारकुशलता की सीढ़ियाँ लगाकर हर कोई जल्दी-से-जल्दी उस पुरानी खुशहाली को दुबारा मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता था...
‘चार पैसे की लड़ाई’ के इस मुश्किल दौर में जब पिता ने अपने आत्मसम्मान के तहत बरसों की बँधी-बँधाई नौकरी बिना किसी विकल्प के इन्तजार किये एकाएक छोड़ दी थी तो दिल्ली के सदर बाजार से आगरे की ‘राजे दी मण्डी’ तक फैली तमाम बिरादरी की आँखें-फटी-की-फटी रह जाना स्वाभाविक था। आश्चर्यजनक यह भी था कि कई वर्षों तक पनाह देने वाले उस कस्बे की ओर पिता ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था और न ही अपने निर्णय को लेकर किसी तरह का कोई अफसोस मन में आने दिया था। इस असाधारण फैसले के बाद घरेलू झगड़ों की आड़ में रिश्तेदारों और सगे-संबंधियों के तमाम चेहरे अजनबियों में तब्दील हो गये थे और बनजारों की सी सहजता से सारा माल-असबाब ट्रक पर लादकर हम सब जयपुर चले आये थे...
जयपुर का वह छोटा-सा किराये का मकान, मिट्टी की मेड़ से घिरा दिगम्बर जैन विद्यालय, मान प्रकाश सिनेमा के सामने गैस के हण्डों तले बिकती गँडेरियों के मोहक ढेर, स्टैच्यू सर्कल की लम्बी, वीरान शामें और झुटपुटे में घर की सीढ़ियों पर हथेलियों के बीच चेहरा टिकाकर बैठे पिता की आकृति...ये सब जयपुर के उस साल भर के प्रवास की पुरअसरार तस्वीरें हैं, जिन्हें भुला सकना मुश्किल हैं। सी स्कीम का वह इलाका, जहाँ हमने अभावों की उस सख्त धूप को झेला था, अब पर्यटकों की गुलाबी नगरी का एक भव्य हिस्सा बन चुका है, जिसमें से उस पुरानी, जर्जर तस्वीर को ढूँढ़ निकालना शायद असम्भव होगा....
दस भूखे आश्रितों का घर चलाने वाले एक अकेले मध्यमवर्गीय पंजाबी के लिए सालभर तक बेकार रहने का मतलब क्या होता है ? शायद बहुत कुछ, परन्तु दुःख और अभाव ने हमें एक अदृश्य सूत्र में बाँध दिया था। पिता के सामने एक वर्ष के दौरान समझौतों के कई अवसर आये, पर वे ‘पंजाबी दी नाक्क’ को पूरी तरह चरितार्थ करते अपनी शर्तों पर जहाँ-के-तहाँ बने रहे और अर्थकेन्द्रित माहौल के आदी बने मेरे अपरिपक्व मन को पहली बार पता चलना शुरू हुआ कि आदमी के माथे पर खिंची आत्मसम्मान की त्यौरियों की कीमत कभी-कभी तमाम भौतिक सुविधाओं से कहीं ज्यादा बैठती है....
और उसके बाद दिल्ली। बेगैरत नकली व्यवहार और हरामजदगियों के बीच बसा एक संस्कृतिविहीन शहर, जैसा कि मुझे हमेशा लगता है। खालीपन के लम्बे अन्तराल के बाद पिता को शिक्षामन्त्रालय में एक सम्मानजनक नौकरी मिल गयी थी और बड़े भाई को यहीं के एक कॉलेज में लेक्चररशिप। दिल्ली में मेरा पहला परिचय सर्दियों की दोपहर में कमलानगर के मेले ग्राउण्ड में फैली ‘चारपाई सभ्यता’ से हुआ था, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति हर दूसरे आदमी की जिन्दगी में खामख्वाह दखल रखता था। तीस हजारी स्थित स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी कैम्पस तक फैली ‘पुराणी दिल्ली’ की वह जिन्दगी कदम-कदम पर बदकारियों से घिरी थी, जिनसे मेरी पुरातनपन्थी माँ मुझे भरकस बचा लेना चाहती थी। एक बार स्कूल के बंगाली दोस्त संदीप सरकार (यह नाम पता नहीं अब तक कैसे याद है) के घर से जब मैं ‘लूचि’ और ‘मांस’ (से मेरी दादी ‘तरकारी’ कहती थीं) खाकर लौटा था तो उन्होंने तीन दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। परन्तु अपनी समूची वैदिक सदाशयता के बावजूद वे मुझे बर्बाद होने से बचा नहीं सकीं। दिल्ली में कुछ ही महीने गुजारने के बाद मैं अपनी गली में ‘बण्टों’ और ‘ठिक्कर’ (सोडावाटर बोतलों के ढक्कनों से खेला जानेवाला खेल। का बेताज बादशाह बन गया था। मुहल्ले का शहरी गाली-गलौज धीरे-धीरे मेरी जबान पर भी चढ़ने लगा सन बावन के आम चुनावों में मैंने भी बच्चों की टोली के साथ ‘चिह्न हमारे डिब्बे का, दीपक दीपक दीपक है’ चिल्ला-चिल्लाकर खासा यश और लाभ अर्जित किया था।
मेरे अपने सांस्कृतिक ‘विकेन्द्रीकरण’ के साथ-साथ घर के दूसरे सदस्यों पर भी महानगर के सुपरिचित दबाव अपना असर दिखाने लगे थे। दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों में धक्के खाने के बाद जब पिता सेक्रेटेरियट से घर लौटते थे तो उन्हें हम बच्चों के साथ अपने अनुभव बाँटने का वक्त ही नहीं मिलता था। यूँ भी बड़े भाई-बहनों की अपनी एक ताजातरीन वयस्क दुनिया थी जिसमें डूब चुकने के बाद उनमें हमारे प्रति एक अनकही हिकारत का सा भाव जागने लगता था। कुल जमा स्थिति यह थी कि सालभर के उस छोटे से अर्से में ही दिल्ली की जहरीली हवा ने हमारे पूरे परिवार के सांस्कृतिक ढाँचे को बेतरह तहस-नहस कर दिया था...माँ इस बीच चोरी-छिपे उस कस्बे की शान्त जिन्दगी को याद कर लेती थीं, जिसे पिता ने एक झटके के साथ तोड़ दिया था और दादी दिल्ली तथा लाहौर के सारे साम्य और ‘जात-बिरादरी’ के पड़ोस के बावजूद ‘सत्तूर मण्डी’ के उस फिक्सेशन से मुक्त नहीं हो पाती थीं जिसके अन्तर्गत लाहौर में हमारी ‘ऐड्डी वड्डी कोठी’ हुआ करती थी। पिता ने अपनी जिन्दगी में हार मानना नहीं सीखा था लेकिन दिल्ली की धक्का-मुक्की और दौड़-भाग उन्हें भी कहीं गहरे में तोड़ने लगी थी।
बचपन के उन दो वर्षों के अनुभव के कारण ही मैं आज तक दिल्ली के नाम से घबराता हूँ क्योंकि कमलानगर की वे घुटनभरी दीवारें ही मेरे लिए इस शहर का पर्याय बन चुकी हैं। दिल्ली का औसत आदमी आज भी मेरे मन में मक्कारी और पंजाबी ‘रिफ्यूजी-सुलभ’ आत्मपरकता की एक पेटेण्ट तश्वीर पेश करता है। रेस्त्राओं और सार्वजनिक स्थलों पर यहाँ लोग तफरीह के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर अपने कपड़ों, अपने पैसों और अपने अक्खड़पन का रौब गालिब करने जाते हैं। चापलूसी और झूठी तारीफ की सतह को नाखून से जरा-सा खुरचते ही यहाँ इन्सान का खुदगर्ज और ‘डॉग ईट डॉग’ वाला बेमुरव्वत चेहरा दिखाई देने लगता है। शायद बँटवारे के बाद के वर्षों में इन लोगों ने यह सारा खुदरापन विकसित किया है, लेकिन स्कूटरों पर ऑफिस बैग लटकाए भीड़ में से गुजरते कुकरेजा, मखीजा, ‘सैक्ट्री साब’, ‘शाहजी‘, ‘होरजी’ और ‘टीटू दी गड्डी’ का यह चलतापुर्जा शहर मुझे कभी रास नहीं आया और न ही शायद कभी भविष्य में आएगा। पुराने दिल्लीवासी माफ करेंगे, लेकिन यदाकदा इस शहर में पहुँचकर जब मुझे नयी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी जाने के लिए ऑटो लेना होता है तो रास्ते भर यह डर बना रहता है कि अभी इसका बददिमाग ड्राइवर किसी अन्धी गली में रिक्शा मोड़कर मुझे मुहल्लेवालों से पिटवा देगा या फिर ‘वन-वे’ का बहाना कर मुझे कनॉट प्लेस से कनॉट प्लेस के सर्कुलर रूट पर चक्कर कटवाता रहेगा।
मेरे बचपन की अधिकांश याद रहने वाली घटनाएँ किसी-न-किसी रूप में यात्रा से जुड़ी है। सम्भवतः यही कारण है कि यात्रा और ‘ट्रांजिशन’ मेरी कहानियों में लगभग एक किरदार की हैसियत से आते हैं। इधर पिछले चार-पाँच वर्षों में काम के सिलसिलें में मैंने इतनी अधिक यात्राएँ की हैं कि नजदीक के लोगों को आश्चर्य होता है। लेकिन इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी सबसे साफ तौर पर याद है कि ट्रेन का वह खूबसूरत सफर, जो हमने दिल्ली से कलकत्ता जाते हुए तय किया था। अलीगढ़ से कुछ आगे रेलवे लाइन के बराबर पक्की दीवार के पीछे फैले अमरूदों के बाग, कानपुर के प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले छोटे-छोटे तिकोने समोसों का स्वाद झाझा स्टेनशन पर आधी रात के वक्त बदले जाते इंजन से आसमान में चाँद पर उठता काला धुआँ और गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर बदहवाश दौड़ते पैरों की आहट....ये सारे बिम्ब मेरे जेहन की तख्ती पर अपनी स्थायी जगह बना चुके हैं...
पिता के तबादले के साथ दिल्ली छोड़कर कलकत्ता आना हम सबके लिए एक विराट अनुभव था क्योंकि सारी गरीबी, खस्ताहाली और गन्दगी के बावजूद कलकत्ता में जिन्दगी की एक उनमुक्त, ताजगीभरी धड़कन थी, जिसे दिल्ली की गला काटने वाली संस्कृति से अलग पहचाना जा सकता था।
आज भी अगर मुझे अपनी गुजरी हुई पूरी जिन्दगी में से कोई छोटा-सा कालखण्ड चुनने के लिए कहा जाए तो मैं बेहिचक हिन्दुस्तान पार्क और बालीगंज में गुजरे उन पाँच वर्षों की खातिर अपनी सारी उम्र को दाँव पर लगाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। कलकत्ता छोड़ने के सोलह लंबे वर्षों के बाद मैं किसी गवेषक की तरह सुधा को साथ लिए उन्हीं परिचित गलियों और सड़कों पर खोये स्मृति चिह्नों की तलाश में बेमतलब यहाँ से वहाँ तक भटका, लेकिन उस गुजरे हुए कालखण्ड को दुबारा जी पाना सम्भव नहीं हुआ। शायद सोलह वर्षों के इस भयावह अन्तराल में वह मासूम दृष्टि, जो जिन्दगी की मामूली खूबसूरतियों को पकड़ पाने के लिए जरूरी होती है, हमसे हमेशा के लिए छीन ली गयी थी...
हिन्दुस्तान पार्क के हमारे दोमंजिला मकान की बगल में खानदानी बंगाली रईसों की एक आलीशान कोठी थी, जिसके लम्बे-चौड़े बगीचे में खूबसूरत गार्डन-चेयर्स पर बैठे मर्द-औरतों के प्रति हम बच्चों के मन में एक अजीब से कौतूहल का भाव जागता था। कौन हैं ये लोग जो सुबह-शाम चाँदी के चमचमाते टी-सेट्स पर चाय पीते हैं और कुर्सी के नीचे हरी घास पर लोट लगाते रोयेंदार कुत्तों का माथा सहलाते हैं। क्या करता है बरामदे की झूलेदार कुर्सी पर बैठकर सिगार पीता वह बूढ़ा, जिसकी बेटी हर रोज रंगीन पाड़ वाली झक्क सफेद कलफ लगी सूती साड़ी पहनकर बेथुन कॉलेज की बस में पढ़ने जाती है। कहाँ गुम हो जाते हैं वे ढेर-ढेर ‘डाब’ जिन्हें छुट्टी वाले दिन माली उस बगीचे के अनगिनत नारियल के पेड़ों से उतारकर घास पर एक कोने में इकट्ठा करता है ? बंगाली आभिजात्य का वह संयत, मगर रौबीला प्रदर्शन हर रोज हमारी आँखों के सामने होता था। और हम हर बार सोचते कि इन खुशकिस्मत लोगों की तरह हमारे घरों में भी क्यों सुबह-शाम बाघबाजार के राजभोगों की हाँडियाँ नहीं आती और क्यों हम भी उन लोगों की तरह दिल बहलाने के लिए घर में तीन-तीन ‘कॉकर स्पेनियल’ कुत्ते नहीं पाल सकते ?
वैसे जिन्दगी हमारी भी ‘दारुण’ मजे की थी, इसमें कोई शक नहीं। घर के बरामदे में एक बड़ा-सा जंगला था जिसके ठीक सामने से एक सड़क आकर हमारी सड़क से मिलती थी। अँग्रेजी के ‘टी’ के केन्द्रबिन्दु पर स्थित घर का बरामदा हमारे लिए घण्टों के लम्बे बालसुलभ मनोरंजन का जरिया बन जाता था। शाम ढलने के बाद जब अँधेरा सिमटता था तो बहन के साथ एक विचित्र होड़ में मैं उस जंगले की सलाखों पर अपना सिर गड़ा लेता था। सामने की एक सड़क से आती कार की हर हेडलाइट के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। कार अगर दायें मुड़ती थी तो ‘प्वाइण्ट’ बहन को मिलता था। और बायें मुड़नेवाली कार मेरे हिस्से में आती थी...
हम बच्चों के लिए बालीगंज लोकल स्टेशन के ओवरब्रिज पर खड़े होकर नीचे से गुजरती ट्रेनों को देखना एक और जरूरी शगल था। हड़ताल वाले दिन रासबिहारी ऐवेन्यू की खुली सड़क के बीचोंबीच ट्रामलाइन की घास पर क्रिकेट जमती थी...इसके अलावा रोइंग क्लब के पीछे झील में बने टापू तक जाते ‘हिलनेवाले पुल’ के नीचे पानी में चने फेंकते ही उन्हें निगलने के लिए छटपटाती सैकड़ों बड़ी-बड़ी मछलियाँ...और गरियाहट चौराहे से देशप्रिय पार्क तक कि वह आये दिन की बिना टिकट ट्राम यात्रा, साउथ एण्ड स्टोर्स के भीतर ताजा घुटी कॉफी की पुरअसरार महक या उससे और आगे गरियाहट के बाजार में बिकते दरियाई कछुओं के रस्सी से बँधे छोटे-छोटे पैर...उस दुनिया ने न जाने कितने सारे अविस्मरणीय अक्स हमारी चमकती आँखों में हमेशा के लिए कैद कर दिये थे...
घोष ब्रदर्स और साउथएण्ड स्टोर्स से कुछ आगे निकलने पर मिलने वाला वह तिकोना पार्क अब भी वहीं है, लेकिन उसके अंदर फैले कूड़े के अस्तव्यस्त ढेर में से कागज तलाशते भिखारियों को देखते हुए अब कहीं भीतर, बहुत गहरे में कुछ टूटता-सा महसूस होता है...
हमारे मकान मालिक एक बुजुर्ग थे, जिनकी पोती एक फालिज के मारे बेटे से हमारी खासी दोस्ती हो गई थी। काली पूजा के दिन उनके घर में बाहर के दरवाजे से लेकर सीढ़ियोंसे होते हुए भी भीतर तक सफेद ‘अल्पना’ से लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाये जाते थे, ताकि दिवाली की रात अगर लक्ष्मी भीतर आने का इरादा रखें तो उन्हें रास्ता ढूढ़ने में कठिनायी न हो। बहुत-सी रातें हमने उस चमत्कारिक देवी की आहटों के इन्तजार में बितायी थीं, लेकिन वे कभी नहीं आयीं और हमारे मकान मालिक ‘दादू’ के मकान की दूसरी मंजिल यूँ ही बरसों तक अधूरी, अधबनी हालत में मरम्मत और पलस्तर का इन्तजार करती रही...
कालीघाट के मोड़ पर जब ट्राम ‘बाटा’ की दुकान के सामने से होती हुई ‘रस्सा रोड’ के स्टॉप पर रुकती थी तो एक बूढ़ा भिखारी अनिवार्यतः ट्राम के जंगले से सट जाया करता था। ‘‘अन्धा के दया करुन, भोगोबान मंगल कोरबे...’’ उसकी परिचित आवाज ट्राम के भीतर गूँजती थी और काली मंदिर की दिशा में संस्कारगत हाथ जोड़ने वाले बंगाली अकसर कुछ-न-कुछ दे देते थे...इस धर्मपरायणता से काफी दूर आठवीं कक्षा के झोपड़ीनुमा क्लासरूम में हमारे सबसे प्रिय अध्यापक उत्पल दत्त (बाद में विख्यात अभिनेता और नाटककार) मुँह में मोटा सिगार दबाये हमें रोनाल्ड रिडआउट की ‘इंग्लिश टुडे’ से अँग्रेजी का पाठ पढ़ाते थे और गाहे-ब-गाहे किसी एक विद्यार्थी को खड़ा कर यह भी पूछ लेते थे कि उसने लाइट हाउस, सिनेमा में लगी ‘यूलिसेस’ फिल्म अब तक क्यों नहीं देखी !..,.यह उत्पल दत्त के ओजस्वी स्वर में सिखाये गये अँग्रेजी साहित्य की विलक्षणताओं के उस पहले सबक का ही चमत्कार था कि मैं रातोंरात बच्चों की परी कथाओं से आगे निकलकर केनेथ ग्रैहम की ‘विण्ड इन दि विलोज’ और विलियम गोल्डिंग की ‘लॉर्ड ऑफ़ दि फ्लाइज’ पर उतर आया था और आगे चलकर हिन्दी माध्यम से हायर सैकेण्ड्री करने के बावजूद मुझे अपनी अँग्रेजी को लेकर कभी हीनता का अहसास नहीं हुआ...
कोई पच्चीस वर्ष गुजर जाने के बाद एक बार जब मैंने प्लेन में अपनी बगल में बैठे शख्स को उत्पल दत्त के रूप में पहचाना था तो मेरे मुँह से अनायास ही ‘गुडआफ्टरनून सर !’ निकल गया था। वे कुढ़कर मेरी ओर पलटे थे और गुस्से से अँग्रेजी में बोले ते कि मैं क्या आपको ‘सर’ दिखाई देता हूँ ? लेकिन जब मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि ‘सर’ सम्बोधन का इस्तेमाल मैंने अपने उस गुरू के लिए किया था जिसने मुझे आठवीं कक्षा में अँग्रेजी सिखाई थी तो वह अनायास ही पिघल गये थे। बम्बई से कलकत्ता की सारी यात्रा के दौरान वे मेरे साथ साउथप्वाइंट स्कूल की उन यादों को ताजा करते थे और फिर आखिरकार दमदम हवाई अड्डे पर जब हम उतरे थे तो चलते-चलते उन्होंने इतने पुरातन ढंग से मेरे सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया था कि मेरे पास उनके पैर छूने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था। उस वक्त लगा था कि चुरुट मुँह में दबाकर अँग्रेजी पढ़ाने वाले उस रौबीले सूटधारी अध्यापक के भीतर कहीं एक अत्यन्त संवेदनशील, दकियानूसी बंगाली का हृदय भी था और बाहर से भीतर तक की यह दुरंगी विविधता ही कमोबेश मेरे बचपन के उस कलकत्ता की वास्तविक पहचान थी...
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book